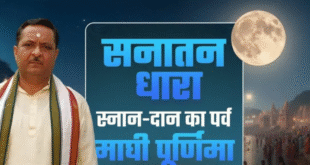पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। इस संहिता में भी आयुर्वेद के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख है। विभिन्न विद्वानों ने इसका निर्माण काल ईसा के 3 हजार से 50 हजार वर्ष पूर्व तक का माना है । इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अत: हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का रचनाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के आसपास या साथ का ही है।
पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है। इस संहिता में भी आयुर्वेद के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख है। विभिन्न विद्वानों ने इसका निर्माण काल ईसा के 3 हजार से 50 हजार वर्ष पूर्व तक का माना है । इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अत: हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का रचनाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के आसपास या साथ का ही है।
चरक : चरकसंहिता के निर्माता चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। कुछ लोग इन्हें कुषाण राज्य का राजवैद्य मानते हैं। किन्तु अधिकांश इतिहासविद् इन्हें पतंजलि के समकालीन ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में मानते हैं। कुछ विद्वान विभिन्न कारणों से पतंजलि और चरक को एक ही मानते हैं। इन्होंने अग्निवेशतन्त्र को व्यवस्थित रूप से सम्पादित, परिवर्धित एवं युगानुरूप उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रतिसंस्कार किया है। इसके बाद अग्निवेशतन्त्र ही चरकसंहिता के नाम से जाना जाने लगा। इसमें दिनचर्या, ऋ तुचर्या आदि स्वस्थ रहने के उपाय और रोग को दूर करने के उपाय बताये गए हैं। इसमें च्यवनप्राश, ब्राह्मरसायन आदि अनेक प्रसिद्ध योग उल्लेखित हैं जो आज भी बनाये जाते हैं और प्रयोग में लिये जाते हैं। इसमें स्वर्ण, रजत, लोह, मण्डूर, शिलाजीत, भिलावा आदि के उपयोग और धातुओं के भस्म प्रयोग का भी संकेत है।
सुश्रुत : शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्साशास्त्री थे। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुतसंहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने दिवोदास धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुतसंहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। सुश्रुत ने आकार भेद से छह प्रकार के यन्त्र बताये हैं। इस तरह के कुल 101 यन्त्रों का उल्लेख इसमें है। सुश्रुत ने 20 प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने आठ तरह के शस्त्रकर्म बताये हैं (जैसे चीरना, फाड़ना, वेधन करना, खुरचना, सीवन करना आदि)। प्रत्येक के आकार और स्वरूप का भी वर्णन किया है तथा इनको बनाने की विधि भी बतार्इ है। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। पट्टी बांधने के चौदह प्रकार बताये हैं। वे आंखों की सर्जरी भी करते थे। उन्हें शल्य क्रिया से प्रसव कराने का भी ज्ञान था। टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उन्हें जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। सर्जरी के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे नशा लाने वाले पदार्थ या विशेष औषधियां देते थे। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाया।
वाग्भट : वाग्भट दो हुए हैं। प्रथम वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह की रचना की। इन्हें वर्तमान में वृद्ध वाग्भट कहा जाता है। इनके पौत्र वाग्भट ने अष्टांगहृदय की रचना की। प्राचीन साहित्यकारों में यही व्यक्ति है, जिसने अपना परिचय स्पष्ट रूप में दिया है। अष्टांगसंग्रह के अनुसार इनका जन्म सिंधु देश में हुआ। इनके पितामह का नाम भी वाग्भट था। ये अवलोकितेश्वर गुरु के शिष्य थे। इनके पिता का नाम सिंहगुप्त था। ये वैदिक धर्मावलम्बी थे। सम्भवत: ब्राह्मण थे, लेकिन इनके गुरु के बौद्ध होने के कारण ये बौद्ध धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे। अष्टांगहृदय का तिब्बती और जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ था। वाग्भट कृत अष्टांगहृदयं के प्रथम अध्याय में ही कफ, वात, पित के साथ जीवनचक्र को जोड़ा गया है। स्वस्थ जीवनशैली हेतु इस किताब में उन्होंने सात हजार सूत्रों की व्याख्या की थी। इन्होंने चरक और सुश्रुत के उपयोगी विषयों का अनुसरण भी किया है।
 Shree Ayodhya ji Shradhalu Seva Sansthan राम धाम दा पुरी सुहावन। लोक समस्त विदित अति पावन ।।
Shree Ayodhya ji Shradhalu Seva Sansthan राम धाम दा पुरी सुहावन। लोक समस्त विदित अति पावन ।।